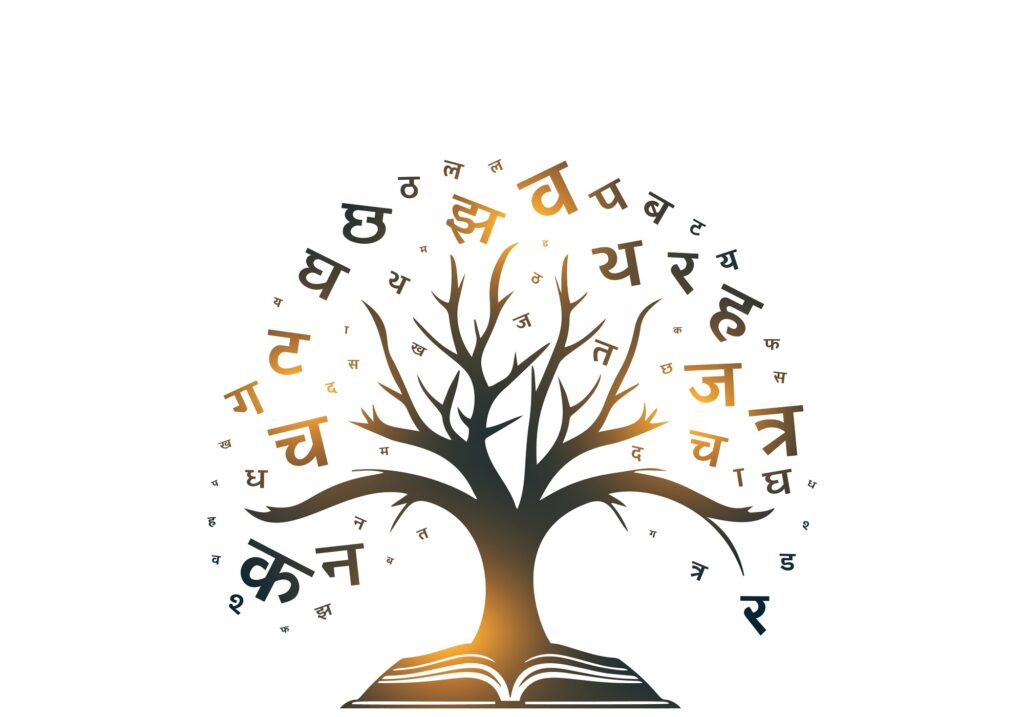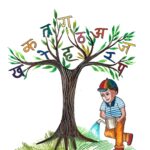हिंदी साहित्य:उद्भव एवं विकास
रजनी प्रभा
हर राष्ट्र की अपनी एक विशिष्टता होती है और भारत की विशेषता है अनेकता में एकता। भारत विविधताओं का देश है। यहां हर धर्म और संस्कृति को जीने वाले लोग अटूट प्रेम,सौहार्द और भाईचारे के साथ रहते हैं।जाहिर तौर पर बहुभाषी राष्ट्र में भाषा संबंधी परेशानियां भी आती हैं। यहां भिन्न-भिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं मगर हिंदी हमारे भारत की राजभाषा है। वैश्विक स्तर पर इसका स्थान हम इसी से सुनिश्चित कर सकते हैं कि_ ”अकेले भारत में 70 करोड़ से ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं और समझते हैं।पूरे ब्रिटेन में जितने लोग अंग्रेजी बोलते हैं,उससे ज्यादा तो अकेले उत्तर प्रदेश में हिंदी बोलते हैं।पूरा पाकिस्तान हिंदी बोलता है। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान,तिब्बत, म्यांमार, अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देशों में भी आपको हजारों से लेकर लाखों लोग हिंदी बोलते और समझते हुए मिल जाएंगे।इसके अलावा फिजी, मॉरीशस,गियाना, सूरीनाम, फ्रीचार्ज ऐसे देश तो हिंदी भाषियों के बसाए हुए ही हैं। दुनियाभर में फैले लगभग दो करोड़ भारतीय लोग भी हिंदी ही बोलते हैं। इसके अलावा लगभग दुनिया के डेढ़ सौ विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाई जाती है।हिंदी समाज का आंकड़ा लगभग डेढ़ सौ की जनसंख्या को छूता है। सच्चाई तो यह है,कि हिंदी केवल अंग्रेजी से नहीं चीनी भाषा से भी आगे है।
हिंदी की प्रसिद्धि को देखते हुए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने अध्यक्षता में घोषणा की थी कि_ ’हिंदी ऐसी विदेशी भाषा है,जिसे 21वी सदी में राष्ट्रीय सुरक्षा और समृद्धि के लिए अमेरिका के नागरिकों को अवश्य सीखनी चाहिए”।1 जो हिंदी विश्वव्यापी है,उसके स्वरूप और विस्तार के बारे में एक से एक विद्वानों ने अपने मत प्रस्तुत किए हैं।खुसरो से लेकर नगेंद्र तक के हिंदी संबंधी विचार हिंदी साहित्य की अनुपम धरोहर हैं। ”हिंदी साहित्य के इतिहास के संदर्भ में दो मौलिक प्रश्नों का समाधान कर लेना आवश्यक है।(1) हिंदी का स्वरूप विस्तार कहां तक है ? (2) हिंदी की सीमा क्या है? हिंदी के स्वरूप विस्तार का प्रश्न कुछ राजनीतिक कारणों से उलझ गया है।हिंदी के विद्वान और अन्य भाषी भी आराम से यह स्वीकार करते हैं, कि भारतवर्ष के जितने भूभाग में वर्तमान हिंदी या खडी बोली सामाजिक व्यवहार अर्थात पत्राचार,शिक्षा, दीक्षा ,सार्वजनिक आयोजन, विचार विनियम तथा साहित्यिक अभिव्यक्ति आदि का माध्यम है।वह सब का सब हिंदी प्रदेश है और उसके अंतर्गत बोली जाने वाली सभी बोलियां हिंदी की उपभाषाएं हैं।इस दृष्टि से वर्तमान में बिहार, झारखंड,उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड,मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान,हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा दिल्ली का इलाका हिंदी क्षेत्र में आते हैं और मैथिली, मगही,भोजपुरी, अवधी, बघेली ब्रज,कनौजी,बुंदेलखंडी, राजस्थानी के विभिन्न रूप कुमाऊनी पहाड़ी बोलियां हिंदी की शाखा प्रशाखा है।यह परिभाषा नई नहीं है। इसका स्वरूप उस समय निर्धारित हो गया था, जब भाषाई राज्य और उनके परिजनों की कल्पना भी नहीं की गई थी।लेकिन इधर यह विवाद जोड़ पकड रहा है। एक सत्य यह है कि हिंदी का अर्थ वर्तमान हिंदी या खड़ी बोली ही है”।2
हिंदी के उद्भव और उसके विकास से संबंधित मतों में
गार्सा द तासी,ग्रियर्सन,शिवसिंह शेंगर,मिश्रबंधु,आचार्य रामचंद्र शुक्ल और नगेंद्र आदि के मत नीव का पत्थर है। डॉ. नगेंद्र के अनुसार_
“हिंदुई”शब्द ’हिंदू+ई’से बना है।हिंदी, हिंदूई या हिंदवी का प्रयोग प्राचीन हिंदी के लिए काफी पहले से मिलता है।तेरहवीं सदी में औफी और अमीर खुसरो ने इसका प्रयोग किया है।’खालिक बारी’ में ’हिंदी और ’हिंदवी’का प्रयोग एक ही भाषा के लिए हुआ है,किंतु ’हिंदी’ का प्रयोग केवल पांच बार है जबकि ’हिंदवी’ का तीस बार।इसका मतलब ये कि पहले ’हिंदी’ की तुलना में ’हिंदवी’नाम ज्यादा प्रचलन में था,धीरेधीरे ’ हिंदवी’ नाम उस भाषा के लिए सीमित हो गया, जिसमे संस्कृत के शब्द अपेक्षाकृत अधिक थे:और ’हिंदुस्तानी’ उस भाषा को कहने लगे जिसमें अरबीफ़ारसी के शब्द ज्यादा थे। ’गार्सा द तासी ’के इतिहास में ’हिंदूई’ तथा ’हिंदुस्तानी’ नाम ठीक इसी अर्थ में आएं हैं।अतः प्राय: केवल ’दक्खिनी ’या ’दक्कखनी’ तथा उसके पहले के उत्तर भारत के मसउद,खुसरो तथा शकरगंजी आदि के साहित्य की भाषा के लिए ही हिंदूई या हिंदवी नाम का प्रयोग करते हैं।”3
शनैः शनैः हिंदी का विकसित स्वरूप वैश्विक स्तर पर उभर कर आने लगा।हिंदी अब बोलचाल की भाषा के साथ साथ संपर्क की भाषा,साहित्य की भाषा और विश्व व्यापार की भाषा का दर्जा पाने लगी है।हिंदी के बढ़ते प्रभाव ने वैश्वीकरण के सपने को साकार किया है,
“आज का युग भूमंडलीकरण_ वैश्वीकरण का युग है, जो भाषा से प्रभावित है। हिंदी भाषा वैश्वीकरण की परिधि में जकड़ गई है। सामाजिक आर्थिक संबंधों में विस्तार, भाषा और साहित्य के विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। वस्तुतः वास्तविक संसाधनों का आदान-प्रदान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की भाषा के विकास का अवसर प्रदान करता है।अब भारत में बहुराष्ट्रीय निगमों के उत्पाद का विज्ञापन हिंदी में हो रहा है। हिंदी आम उपभोक्ता की भाषाएं गार्जियन एडिनबरा अंतरराष्ट्रीय टेलीविजन समारोह, के अवसर पर मर्डोक जूनियर ने चेतावनी देते हुए कहा था कि_ ”अंग्रेजी की सबसे कठोर प्रतिद्वंदी भाषा के रूप में हिंदी और सामने आ रही है।”4
यह कथन हिंदी के अंतर्राष्ट्रीय भाषा होने का प्रमाण है।हिंदी की निरंतर प्रगति और बढ़ते प्रभाव को देखते हुए इसे शीघ्र ही राष्ट्रभाषा का दर्जा मिल जाना चाहिए।
” वैश्विक स्तर पर भाषा के प्रभाव के बारे में _ 13 जुलाई 2007 को न्यूयार्क में आयोजित आठवें विश्व हिंदी सम्मेलन का केंद्रीय विषय ही ’विश्व मंच पर हिंदी’ रहा था।जिसमें विदेशों में हिंदी शिक्षा, विदेशों में हिंदी साहित्य सृजन, हिंदी के प्रचारप्रसार में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका,वैश्वीकरण,मीडिया और हिंदी के प्रचार-प्रसार में फिल्मों की भूमिका,हिंदी युवा पीढ़ी और ज्ञान-विज्ञान हिंदी भाषा और साहित्य,साहित्य के अनुवाद की भूमिका आदि विषयों पर प्रस्तुत विचार,परिचर्चाएं,सुझाव,निर्णय आदि विश्व में हिंदी का स्थान दिलाने में अग्रसर दिखाई देते हैं। मतलब 21वीं सदी में हिंदी पूर्वी पश्चिमीकरण के मध्य एक भावात्मक सेतु के रूप में साबित होगी।और इतना ही नहीं वह वैश्विकभाषा के रूप में भी सामने आएगी। वैसी भाषा बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 देशों में दो तिहाई बहुमत की यानी 129 देशों के समर्थन की आवश्यकता है।विश्व योग दिवस संबंधी प्रस्ताव पर 177 देशों की सहमति दर्ज कराई जाती है ,जिससे उम्मीद बढ़ी है कि आने वाले दिनों में हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा का दर्जा हासिल होने में मुश्किल नहीं आएगी”।5
बूंद बूंद से घड़ा भरता है।एक एक प्रयास हिंदी की प्रगति में सहायक सिद्ध होगा। इसके लिए कोशिश करें,कि अपने जीवन में हिंदी को पूर्णत:आत्मसात करें।लिखनेबोलने से लेकर देखनेसुनने तक के लिए केवल और केवल हिंदी का ही प्रयोग करें।
”हिंदी शब्द का संबंध संस्कृत शब्द ’सिंधु’ से माना जाता है। ’सिंधु’सिंधु नदी को कहते थे और उसी आधार पर उसके आसपास की भूमि को ’सिंधु’कहने लगे। हिंदी शब्द ईरानी में जाकर ’हिंदू’ और फिर हिंद हो गया और उसका अर्थ हो गया ’सिंध प्रदेश’ का। बाद में ईरानी धीरे-धीरे भारत के अधिक भागों से परिचित होते गए और इस शब्द के अर्थ में विस्तार होता गया तथा हिंदी शब्द धीरे-धीरे पूरे भारत का वाचक हो गया।इसी में ईरानी के ’ईक’प्रत्यय के लगने से ’हिंदीक’ बना, जिसका अर्थ है ’हिंद का’। यूनानी शब्द ’इंदिका’या अंग्रेजी शब्द ’इंडिया’इसी के विकसित रूप हैं। ’हिंदीक’भी हिंदी का ही परिवर्तित रूप है और इसका मूल अर्थ है ’हिंद का’। इस प्रकार यह विशेषण है,किंतु भाषा के अर्थ में संज्ञा हो गया है। हिंदी भाषा के लिए इस शब्द का प्राचीनतम प्रयोग शरफुद्दीन यज्दी के ’जफरनामा’ (1424) में मिलता है। ’हिंदी’शब्द का प्रयोग आज मूलतः 3 अर्थों में हो रहा है: 1) ’हिंदी’शब्द अपने विस्तृततम अर्थ में हिंदी प्रदेश में बोली जाने वाली 17 बोलियों का घोतक है। हिंदी साहित्य के इतिहास में ’हिंदी’ शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में होता है, इसीलिए इसके अंतर्गत ब्रज, अवधी, डींगल, मैथिली,खड़ी बोली आदी प्राय: सभी में लिखित साहित्य का विवेचन किया जाता है। 2) भाषा विज्ञान में प्राय: ’पश्चिमी हिंदी’और ’पूर्वी हिंदी’को ही हिंदी मानते रहे हैं। ग्रियर्शन ने इसी आधार पर हिंदी प्रदेश की अन्य उपभाषाओं को राजस्थानी, पहाड़ी,बिहारी कहा था, जिनमें ’हिंदी’शब्द का प्रयोग नहीं है, किंतु अन्य दो को हिंदी मानने के कारण ’पश्चिमी हिंदी’ तथा ’पूर्वी हिंदी’ नाम दिया गया था। इस प्रकार इस अर्थ में ’हिंदी’ आठ बोलियों (ब्रज, खड़ी बोली ,बुंदेली, हरियाणवी,कनौजी, अवधि, बघेली,छत्तीसगढ़ी)का सामूहिक नाम है। 3) ’हिंदी’शब्द का संकुचित अर्थ है: खड़ी बोली साहित्यिक हिंदी, जो आज हिंदी प्रदेशों की सरकारी भाषा है, पूरे भारत की राजभाषा है, समाचारपत्रों और फिल्मों में जिसका प्रयोग होता है, जो हिंदी प्रदेश में शिक्षा का माध्यम और जिसे ’परिनिष्ठित हिंदी’, ’मानक हिंदी’, आदि नामों से अभिहित करते हैं।”6 महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने ’हिंदी भाषा’के प्रयोग के संबंध में यह मत व्यक्त किया है” इस प्रकार दसवीं से 14वीं शताब्दी के मध्य जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, ’अपभ्रंश’ का ही बढ़ाव है।’अपभ्रंश’ के इसी बढ़ाव को कुछ लोग ’उत्तर कालीन’अपभ्रंश कहते हैं,कुछ ’पुरानी हिंदी’। यद्यपि अपभ्रंश अपने मूल रूप में 14वी शताब्दी में ही आ गया था।15वीं शताब्दी तक ’हिंदी’साहित्य की भाषा बनी रही, तथापि 18वीं शताब्दी तक बोलचाल की भाषा पृथक हो उसके समानांतर साहित्य रचना का माध्यम बन गई थी।
” आचार्य चंद्रकिशोर पराशर ने हिंदी भाषा के विकास में जिन दो माध्यमों की चर्चा की है, उनमें एक है ,भाषा और मीडिया तथा दूसरा भाषा और सिनेमा। भाषा और मीडिया के संबंध में वे लिखते हैं, कि ’संचार क्रांति के इस युग में मीडिया किसी भी भाषा के अस्तित्व के प्रसार का मुख्य माध्यम है। भारत की स्वाधीनता के पूर्व हिंदी को प्रचारित प्रसारित करने में हिंदी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही।वस्तुत:पत्रपत्रिकाएं ही वे माध्यम हैं, जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रीय संवाद करने का माध्यम बनाया और सुदूर गांवोंकस्बों तक हिंदी की पहुंच सुनिश्चित कराई।बाद में जब वीडियो नेट प्रसारमाध्यम के रूप में आया, तो उसने भी हिंदी को समाचार व मनोरंजन का माध्यम बनाया और पढ़े-लिखे शहरी वर्ग से लेकर ग्रामीण भारत तक में रह रहे अपेक्षाकृत कम पढ़े _लिखे अथवा अनपढ़ वर्ग तक को प्रभावित करना प्रारंभ किया।”7
”खड़ी बोली हिंदी का उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है,किंतु यदि ’हिंदी’को ’पश्चिमी हिंदी’ और ’पूर्वी हिंदी’की आठ बोलीयों का प्रतिनिधि माने तो उसका उद्भव शौरसेनी तथा अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। विस्तार में जाकर यदि 17 बोलियों का प्रतिनिधि माने तो हिंदी का उद्भव शौरसेनी,अर्धमागधी तथा मागधी अपभ्रंश से हुआ है।
यों तो हिंदी भाषा के कुछ व्याकरणिक रूप पाली में ही मिलने लगते हैं,प्राकृतिक काल में उनकी संख्या और भी बढ़ गई है है तथा अपभ्रंश काल में यह रूप 40% से भी ऊपर हो गए हैं, किंतु हिंदी भाषा का वास्तविक
आरंभ 1000 ईस्वी से माना जाता है।इस तरह हिंदी के विकास का इतिहास आज तक कुल लगभग 10 सौ वर्षों (1000_ 2000)में फैला है। भाषा के विकास की दृष्टि से इस पूरे समय को तीन कालों में बांटा जा सकता है_ आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल।”8
आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक ये हिंदी सेवियों की ही महती सेवा रही है,की आज हिंदी को अपना व्याकरण तक मिल चुका है।
यों तो आदिकाल में ही हिंदी का व्याकारणिक स्वरूप भी उजागर हो गया था तथापि प्रयोजनमुलक हिंदी और भाषाविज्ञान का परिष्कृत स्वरूप धरने में इसे इतना समय लग गया।
” साहित्यिक सामग्री का सोशल मीडिया के जरिए प्रकाशन जैसे-जैसे आसान हुआ, उसी अनुपात में साइबर संसार में साहित्यिक सामग्री की मात्रा और गुणवत्ता में भी बदलाव आए। बहुत से लेखक कवि जिन्होंने सोशल मीडिया पर ही अपने लेखन की छोटी सी शुरुआत की थी,वह जाने पहचाने नाम बन चुके हैं।इस तरह हम देखते हैं कि सोशल मीडिया साहित्यकारों के लिए वरदान साबित हुआ है,लेकिन इसका एक और पहलू भी है।बहुत से आलोचक कहते हैं कि सोशल मीडिया की वजह से नई रची जा रही सामग्री की गुणवत्ता में गिरावट आई है।इसके विपरीत यह बात काफी हद तक तथ्यात्मक है, की सोशल मीडिया में प्रकाशित होने वाली सामग्री पर कोई संपादकीय बंधन नहीं होता है। प्रकाशन से पहले लेखक अपनी रचना को बार-बार मंजाकर उसे और अधिक चमकाने का धीरज खो रहा है। यह स्वभाविक है कि ’लाइक्स’ और पोस्ट पर होने वाली चर्चाऐं लेखक को प्रोत्साहित करती है, कि वे जल्द पोस्ट करें। फेसबुक एक तेजप्रवाह वाली नदी की तरह है,जिसमें इसके प्रयोक्ता भी उसी गति से बहते रहते हैं।”9
आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक दिनब दिन हिंदी साहित्य निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर होता रहा है।एक से एक उत्कृष्ठ महाकाव्य,खंडकाव्य,प्रबंध काव्य,उपन्यास,कहानी,कविता आदि हिंदी की विजय गाथा की घोतक है।ऐसी वैश्विक स्तर पर कायम भाषा को अपने ही राष्ट्र की राष्ट्रभाषा का दर्जा देने में संशय और देर क्यों।हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा होने का संपूर्ण अस्तित्व रखती है।
संदर्भ
(1)पुस्तकहिंदी और देवनागरी (प्राचार्य डॉ.शहाबुद्दीन शेख गौरव ग्रंथ) संपादकडॉ.हनुमंत जगताप
लेखकडॉ.अशोक श्रेपद गायकवाड़(अहमदनगर) संस्करणप्रथम,पृष्ट संख्या_20
(2)
पुस्तक_ हिंदी साहित्य का इतिहास
संपादक/_डॉ.नगेंद्र/डॉ हरदयाल
संस्करण77/78 वा 2021,पृष्ठ संख्या 1
(3) वही पूर्व/पृष्ठ संख्या_10
(4)साहित्य अमृत_जुलाई2008,विश्व हिंदी सम्मेलन विशेषांक,पृष्ठ संख्या_15
(5)साहित्य अमृतअक्टूबर2015, पृष्ठ संख्या_117 (6) पुस्तकहिंदी साहित्य का इतिहास
संपादक_डॉ.नगेंद्र/डॉ.हरदयाल
संस्करण_77/78वा 2021, पृष्ठ संख्या_11/12
(6) राष्ट्रभाषा संदेश, प्र. सं.विभूति मिश्र,जुलाई 2016 पृष्ठ संख्या_07
(7) पुस्तकहिंदी साहित्य का इतिहास संपादकडॉ. नगेंद्र/डॉ.हरदयाल
संस्करण77/78 वा 2021,पृष्ठ संख्या_12 (9) हंस पत्रिकासं.संजय सहाय.
वर्ष_33,अंक_2 सितंबर 2018,पृष्ठ संख्या_34